राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना करें। (Describe the liberal views of political science.)
राजनीतिक चिन्तन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राज्य और राजनीति के प्रति उदारवादी मार्क्सवादी दर्शन है। जो विभिन्न दर्शन प्रतिपादित किये गये उनमें सबसे प्रमुख उदारवादी दर्शन, 17वीं सदी से लेकर अब तक पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तन पर छाया रहा। पश्चिमी यूरोप के देश इंगलैण्ड और अमेरिका पर इसका प्रभाव सबसे अधिक हुआ। प्रारम्भ में उदारवाद केवल मध्यम वर्ग विशेष तथा व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन था। परन्तु, बाद में इसने एक ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के दर्शन में परिवर्तित होने का प्रयास किया, जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना हो गया।
उदारवादी दर्शन के दो रूप है, प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद और दूसरा आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद।
1. प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद:- उदारवाद मुख्यतया यूरोप की दो महान क्रांतियों सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म-सुधार की उपज है। 17वीं शताब्दी में हॉब्स और लॉक के राजनीतिक चिन्तन के साथ इसका उदय हुआ। 18वीं और 19 वीं सदी में पराम्परागत उदारवाद ने अनेक अवसरों पर प्रगति किया। उदारवादी चिन्तन ने दास प्रथा पर प्रहार किया और इस प्रकार मानवीय स्वतंत्रता तथा समानता की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उसने संसदीय संस्थाओं में सुधार और वयस्क मताधिकारी को अपनाने पर जोर दिया जिनके आधार पर इंगलैंड में चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन हुआ, मजदूरों की दशा में सुधार के प्रयत्न किये गये और नये औद्योगिक नगरों को लोक सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ ।
2. आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद :- उदारवादी दर्शन ने मार्क्सवादी चिन्तन को तो लगभग सम्पूर्ण अंशों में ठुकरा दिया, परन्तु उसने आदर्शवाद के साथ. सामंजस्य करते हुए अपने विचारों को संशोधित किया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में प्रतिपादित उदारवाद के इस नवीन तथा सामंजस्यकारी रूप को ही नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया।
मिल ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के लिए प्रयल किया जाना चाहिए। समाज की उत्पादन क्षमता और मानवीय साधनों को पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और इस संबंध में उसके राष्ट्रीय समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी विरोध नहीं किया गया।
ग्रीन ने उदारवाद को इतना विस्तृत कर दिया कि उसमें राज्य के सभी महत्त्वपूर्ण हितों का समावेश हो सकता था। इस प्रकार आधुनिक उदारवाद लोकतंत्र तथा लोककल्याणकारी राज्य का पर्यायवाची बन गया।
उदारवादी दर्शन के प्रमुख लक्षण-
1. उदारवादी दर्शन का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति है:- उदारवादी दर्शन का केन्द्रीय तत्त्व व्यक्ति है। हॉब्स तथा लॉक व्यक्ति से ही अपना चिन्तन प्रारंभ करते हैं। ये समाज से पृथक् व्यक्ति और उसको प्रकृति को अपने दर्शन का आधार बनाते हैं। ग्रीन का विचार है कि व्यक्ति अपने अन्तःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करता है।
2. मानवीय विवेक में आस्था:- उदारवादी दर्शन का एक प्रमुख तत्त्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। उदारवादी इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक की प्रधानता दी जानी चाहिए। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्रा चिन्तन को प्रोत्साहित किया।
3. व्यक्ति साध्य और समाज तथा राज्य साधन:- उदारवादियों के लिए व्यक्ति का भौतिक बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण तथा उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास हो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चीज है। समाज और राज्य तो साधन मात्र है और उनका महत्त्व उसी सीमा तक है जहाँ तक वे इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं।
4 सजनीति की जड़ें- सामाजिक विविधताओं में हैं:- उदारवादी विचारक राजनीति को किसी वर्ग विशेष का बपौती नहीं मानते। इनके विचार से राजनीति की जड़ें सामाजिक विविधताओं में है। उदारवादी इन विविधताओं को समाप्त करने की बात नहीं सोचते वरन् इन विविधताओं में एकता के समर्थक है। मिलर के शब्दों में राजनीति जारी रहेगी क्योंकि विविधताएँ समाप्त होने वाली नहीं है। राजनीतिक का अस्तित्व इन सामाजिक विविधताओं में निहित है।
5. धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श:- उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
6. मानवीय स्वतंत्रता की धारणा और मानवीय अधिकारों में अटूट विश्वास:- वस्तुतः उदारवाद का उदय ही मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ है। उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है। ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते रहे हैं।
7. शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन:- उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं वरन् कानून की प्रधानता होनी चाहिए। इस प्रकार उदारवादी राजनीति संविधानवादी राज्य की राजनीति है।
8. लोकतंत्र और लोकतांत्रिक पद्धति में अटूट विश्वास:- उदारवाद का जन्म तानाशाही शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का मूल तत्त्व है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्रता उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों पर उनकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है।
9. अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास:- उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शनैः-शनै और शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए। उसे अन्य राष्ट्रों की प्रगति में भी सहायता करनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार राष्ट्रीय वैमनस्य की भावना को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और राज्यों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।
आलोचना:- 1914 के प्रथम महायुद्ध तक सारे यूरोप में उदारवाद का बोलवाला था परन्तु भयानक विश्वयुद्ध के दौरान रूस में समाजवादी क्रांति, जर्मनी में तानाशाही व्यवस्था का उदय और 1930 का आर्थिक संकट आदि कुछ ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय कारण थे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा को आघात पहुँचाया। 19वीं सदी में इसे क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा समझा जा रहा था। 20वीं सदी में उसे क्रांति विरोधी और यथास्थिति की रक्षक विचारधारा कहा जाने लगा। आज उदारवाद की निम्न आधार पर आलोचना की जाती है
1. इतिहास व परम्पराओं की अपेक्षा अनुचित:- वर्क के अनुसार उदारवादी विचारधारा सर्वप्रथम इस कारण आलोच्य है कि वे समाज के रूप के संबंध में इतिहास व परम्पराओं के उचित महत्त्व को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि सभी मानव संस्थाएँ ऐतिहासिक विकास का परिणाम होती है। अनुदारवादियों के अनुसारः अतीत से संबंध न तो एकाएक तोड़ा ही जा सकता है और न ऐसा करना वांछनीय है।
2. राज्य को कृत्रिम व यांत्रिक मानना त्रुटिपूर्ण:- अनुदारवादियों के अनुसार उदारवादी विचारधारा इसलिए भी आलोच्य है कि वह समाज व राज्य के रूप को कृत्रिम व यांत्रिक मानती राज्य व्यक्तियों द्वारा निर्मित की गई किसी संविदा से बना हुआ है। राज्य व्यक्ति की सामाजिक पद्धति का एक विकसित रूप है जो कृत्रिम न होकर स्वाभाविक है।
3. व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार त्रुटिपूर्ण है:- आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार उदारवाद की यह मान्यता भी सही नहीं है कि व्यक्ति का कल्याण उसे पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देने में है। उनके अनुसार व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता से किसी की भी स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड देने का अर्थ व्यक्तियों की मनमानी पर आधारित अराजकता की व्यवस्था हो सकती है।
4. राज्य द्वारा नियमित स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है:- आदर्शवादियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदत्त व नियमित स्वतंत्रता हो सकती है। उनके अनुसार व्यक्ति का व्यक्तित्व राज्य के व्यक्तित्व का एक अंग होता है तथा उसके विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाय तथा उनकी स्वतंत्रता को सीमित किया जाय।
5. मार्क्सवादियों द्वारा आलोचना:- मार्क्सवादियों के अनुसार उदारवाद द्वारा प्रतिपादित खुद प्रतियोगिता से समाज सम्पन्न व विपन्न लोगों के दो वर्गों में बँट जाता है जिससे सभी व्यक्तियों का वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं रहती वरन् वह सम्पन्न लोगों को ही प्राप्त होती है। प्रतियोगिता मूलक लोकतंत्र में भी शासन की शक्ति पूँजीपति वर्ग के हाथों में रहती है। उनसे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होता है।
उदारवाद की एक लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वाधीनता, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का दर्शन समझा जाता रहा है। उदारवाद बदली हुई परिस्थितियों में समाजवाद और मार्क्सवाद की चुनौती के सम्मुख एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में बना रहेगा। यह आनेवाले कल का महत्त्वपूर्ण प्रश्नचिह्न हैं।


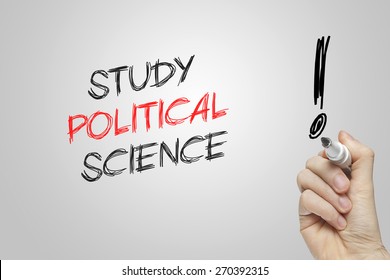




0 Comments